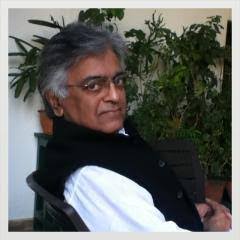डॉ. परिवेश मिश्रा
रायगढ़ ज़िले में औद्योगिक विकास की कहानी शुरू हुई जब 23 वर्षीय राजा चक्रधर सिंह के द्वारा उपलब्ध करायी गयी लगभग चालीस एकड़ भूमि पर एक जूटमिल की स्थापना की गयी। यही मिल आगे चलकर रायगढ़ में नये उद्योगों की स्थापना में ऐसा रोड़ा बन गयी जिसे हटाते 1980 की दशक बीतने लगा था। कहानी की शुरुआत दरअसल तब हुई जब 1897 में अपने पिता बिहारीलाल की उंगली पकड़े पांच वर्षीय बालक पालूराम ने हरियाणा के अकालग्रस्त इलाके के धनाना गांव से निकल कर रायगढ़ में पैर रखे थे। उसी काल में पास के गांव लोहारी से निकल कर उनकी बुआ के बेटे किरोड़ीमल कलकत्ता पहुंचे थे। बीसवीं सदी के शुरुआती दशकों तक सेठ किरोड़ीमल अनुभव, नाम और पैसा कमा चुके थे। इधर सेठ पालूराम धनानिया रायगढ़ में अपने पिता के शुरू किये धान के कारोबार में जम चुके थे। हरियाणा से निकलने के लगभग तीस वर्षों के बाद मामा-बुआ के इन बेटों ने मिलकर रायगढ़ के पहले उद्योग की शुरुआत की। सन् 1928 में सेठ किरोड़ीमल ने यहाँ जूट मिल की स्थापना की और पालूराम धनानिया ने प्रबंधन सँभाला।
सारंगढ़, रायगढ़ और उदयपुर (धर्मजयगढ़) राज्यों के इलाकों में पटसन की पैदावार काफी थी। हालांकि इतनी भी नहीं थी कि मिल की सतत् आवश्यकता पूरी कर सके। किन्तु एक फ़ैक्टर और था। पूरे मध्य तथा उत्तर-मध्य भारत में उन दिनों कोई जूट मिल नहीं थी। जबकि बारदाने की आवश्यकता सबको थी। इसलिए यदि कुछ अतिरिक्त पटसन बंगाल (तब बांग्लादेश का हिस्सा भी भारत में था) से आयात किया जाता तो भी सौदा मुनाफ़े का ही बैठता था। यहां तक सोच में कोई खामी नहीं थी। किन्तु मिल चल नहीं पायी। कहते हैं इतिहास से सबक न लेने पर इतिहास अपने आप को दोहराता है। इतिहास बना था असम में और इसने अपने आप को दोहराया रायगढ़ में। सन 1820 के दशक में ईस्ट इंडिया कम्पनी के अधिकारी रॉबर्ट ब्रूस ने असम के ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में स्वाभाविक रूप से उपजे हुए चाय के पौधे देखे। यह तब की बात है जब चीन से अफ़ीम के बदले चाय लेकर इंग्लैंड और योरोप भेजते हुए कई दशक बीत चुके थे। उधर ब्रिटेनवासियों को चाय की लत लग गयी और इधर चीन ने अंग्रेज़ों से अफ़ीम के स्थान पर नगद की मांग रख दी। चाय अंग्रेज़ों के लिए अचानक बहुत महंगी हो गयी।
रॉबर्ट ब्रूस की खोज की खबर से उत्साहित ईस्ट इंडिया कम्पनी ने चाय के व्यावसायिक उत्पादन का फ़ैसला कर लिया। चाय बागान शुरू कर दिये गये। लेकिन प्रयोग असफल हो गया। श्रमिक आधारित इस प्रोजेक्ट की योजना बनाते समय कम्पनी मान कर चली थी कि स्थानीय श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो जायेंगे। और चूंकि स्थानीय होंगे सो अपने रहने खाने की व्यवस्था भी स्वयं कर ही लेंगे। हकीकत कुछ और साबित हुई। असमिया ग्रामीण सदियों से चली आ रही अपनी जीवनशैली में रातों रात परिवर्तन लाने के लिए बिल्कुल उत्सुक नहीं थे। दूसरों के नियंत्रण में उन्होने कभी काम नहीं किया था। कुछ लोगों ने काम शुरू भी किया तो हर दूसरे दिन उन्हें घर और खेत की याद सताती। चार दिन की छुट्टी लेकर जाते तो चौदह दिन में लौटते। अनेक लौटते ही नहीं। अंत में आजिज़ आकर ईस्ट इंडिया कम्पनी ने हाथ उठा दिये। इसके बाद दो बातें हुईं। 1839 में चाय उत्पादन का काम नये मालिक “असम कम्पनी” के हाथों में सौंपा गया। पिछले मालिक के अनुभवों से सबक लेकर जो काम असम कम्पनी ने सबसे पहले किया वह था श्रमिकों को बाहर से लाकर बसाने का। श्रमिक सप्लाय करने के लिये ठेकेदारों को नियुक्त किया गया। यहीं से शुरुआत होती है छत्तीसगढ़, झारखण्ड, छोटा नागपुर, और आंध्र प्रदेश जैसे इलाकों से ले जाये गये श्रमिकों की कहानी। कालांतर में ये “टी-ट्राईब” के नाम से जाने गये।
“टी-ट्राईब” के पहुंचने के बाद नित नये फैलते बागानों को स्थायी मज़दूर मिले। अपनी जड़ों से उखड़कर गये लोग पूर्णकालिक श्रमिक बने और बागान मालिकों के लिए ज़रूरी हो गया कि इनके रहने खाने आदि की व्यवस्था करें। और चाय बागान का कारोबार चल निकला। अब वापस चलें रायगढ़ की जूट मिल पर। सेठ-द्वय किरोड़ीमल और पालूराम ने नयी और महंगी मशीनें लगवा कर मिल खड़ी की, बाज़ार ढूंढ़ा और बढ़ाया, लेकिन श्रमिकों की उपलब्धता की जिस आश्वस्ति (या उम्मीद) पर यह सब किया था वह गलत साबित हुई। किसी औद्योगिक इकाई में कार्य करने का पूर्वानुभव न होने के चलते स्थानीय श्रमिकों में कार्य-अनुशासन नहीं था। स्थानीय किसानों को पटसन की पैदावार बढ़ाने की ओर प्रेरित करने के प्रयास भी सफल नहीं हुए। लागत बढ़ना और मुनाफे पर चोट पड़ना स्वाभाविक था। हो सकता है और भी कारण रहे हों। 1935 में रायगढ़ की जूट मिल बिक गयी। खरीदने वाले थे कलकत्ता के सेठ सूरजमल जालान और सेठ नागरमल बजौरिया। आगे चलकर रायगढ़ जूट मिल एक बार और बिकी। इस बार भी खरीददार मारवाड़ी ही थे (श्री पवन कुमार अग्रवाल) और वे भी कलकत्ते के ही रहने वाले थे।
कलकत्ता और मारवाड़ियों का जूट और जूट मिलों से पुराना संबंध रहा है। पूर्वी भारत पारम्परिक रूप से पटसन पैदा करता रहा है। लेकिन भारत में इस पटसन से जूट बनाने की कोई मिल नहीं थी। सारा जूट ब्रिटेन से आयात होता था। ब्रिटेन की सारी जूट मिलों का कच्चा माल रूस से आता था। 1850 के आसपास एक युद्ध हुआ (क्रायमियन वॉर) जिसमें एक ओर रूस था और दूसरी ओर ब्रिटेन समेत दूसरे देश। स्वाभाविक था इस परिस्थिति में पटसन और अलसी के बीज का ब्रिटेन पहुंचना बंद हो गया और भारतीय पटसन की पूछ बढ़ गयी। बीसवीं सदी के शुरुआती दशकों में मिलों, कम्पनियों और फ़र्मों के मालिकों के बीच खरीद बिक्री की उथल पुथल रही थी। इसका एक कारण था 1913 से प्रभाव में आया कम्पनी एक्ट। हालांकि तब तक ज़्यादातर फ़र्म ट्रेडिंग का काम ही करती थीं। मैनुफैक्चरिंग में कम लोग थे। इन दशकों में मारवाड़ियों ने अंग्रेज़ों के अधिपत्य में रहा बहुत सा कारोबार खरीदा और बढ़ाया। इनमें ट्रेडिंग फ़र्मों के साथ साथ अनेक जूट मिल, कोयला खदान, तेल मिल आदि भी शामिल थीं।
1938 में सेठ सूरजमल की मृत्यु हो गयी (सेठ नागरमल की पहले हो गयी थी)। उन्ही दिनों दूसरा विश्वयुद्ध भी शुरू हो गया और रायगढ़ में काम ढंग से शुरू करना आगे टलता रहा। नयी व्यवस्था में सूरजमल के बड़े बेटे मोहनलाल जालान ने अपने भाईयों बंशीधर, बैजनाथ तथा सेठ नागरमल के बेटों के साथ काम संभाला था। रायगढ़ जूट मिल बाद में मोहन जूट मिल के नाम से जानी गयी। उन्होने स्थानीय प्रबंधन के लिए सेठ मांगीलाल भंडारी को एजेन्ट और श्री सरावगी को मैनेजर नियुक्त किया। श्रमिक उपलब्धता का समाधान उनके पास पहले से था। कलकत्ता की इनकी मिलों में गोरखपुर के रामसुभग सिंह इस काम के प्रभारी थे और “बड़े- सरदार” कहलाते थे। उनके साथ कलकत्ता में काम कर रहे गोरखपुर और आज़मगढ़ के अलावा बिहार के छपरा के मजदूर रायगढ़ लाये गये (और फिर वे यहीं रच-बस गये)। आज़ादी के शुरुआती सालों में कांग्रेसी सरकार को मध्यप्रदेश की इस इकलौती जूट मिल के महत्व का अहसास था। श्रम मंत्री रहे श्री गंगाराम तिवारी और श्री वी.वी. द्रविड़, दोनों को इंदौर की मिलों में श्रमिक नेता के रूप में काम करने का अनुभव था और रायगढ़ ज़िले के स्थानीय मंत्री सारंगढ़ के राजा नरेशचन्द्र सिंह के साथ इनका अच्छा तालमेल था। इन सब की निगरानी मे मजदूरों के लिए घर बने, सब घरों को बिजली, पानी, शौचालय की सुविधा मिली। खाना पकाने के लिए केरोसिन जैसी चीज़ें मुफ़्त दी गयीं। अन्य हितों की व्यवस्था हुई।
1950 के दशक में मिल में काम करने की इच्छा से आये हुए अनुभवी मजदूर थे। देश और प्रदेश में संवेदनशील और प्रगतिशील सरकारें थीं जो औद्योगिकीकरण भी चाहती थी और मजदूरों का हित संरक्षण भी। मजदूर और मिल मालिक के बीच बैलेंस बनाने में सक्षम मंत्री और विधायक सरकार में थे। रायगढ़ के एकमात्र उद्योग की गाड़ी चल निकली। पर बहुत आगे नहीं बढ़ पायी। अब की बार न तो मिल घोषित रूप से “बंद” हुई न ही चालू रह पायी। जूट मिल रायगढ़ के लिए धीरे- धीरे एक शो-पीस बन कर रह गयी। उन्नीस सौ अस्सी के दशक की शुरुआत में भारत सरकार ने एक नयी औद्योगिक नीति की घोषणा की। इसका मुख्य फ़ोकस था देश के पिछड़े और उद्योग रहित ज़िलों में औद्योगिक विकास करने पर। साथ ही ज़ोर था यथासंभव ऐसे समूहों को प्रोत्साहित करने पर जहां एक ही क़िस्म के उद्योगों की संभावना हो। सरकार द्वारा चयनित स्थानों में नये उद्योग स्थापित करने वालों के लिए सरकार की ओर से अनेक ऐसे प्रस्ताव (या प्रलोभन) दिये गये जिन्हें कालांतर में सामूहिक रूप से “फ़्री-बीज.” कहा गया। मध्यप्रदेश में भी इस नीति के लाभ प्राप्त करने के प्रयास शुरू हुए। नये उद्योग शुरू करने वालों के लिए राज्य की उन दिनों की आर्थिक राजधानी इन्दौर पसंदीदा जगह थी। किन्तु नयी नीति की परिधि में विकसित इंदौर नहीं आ सकता था। इसलिए सन् 1983 में इंदौर से बाईस किलोमीटर दूर, किन्तु ज़िले की सीमा के पार, उद्योग रहित ज़िले धार के पीथमपुर गाँव का चयन किया गया। आज पीथमपुर में ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। इसी कड़ी और दौर में भोपाल के पास, लेकिन रायसेन ज़िले का, मंडीदीप; ग्वालियर के पास किन्तु मुरैना ज़िले का बानमोर और अन्य अनेक स्थानों में औद्योगिक विकास हुआ। रायपुर के पास उरला, बिलासपुर के पास सिरगिट्टी जैसे अनेक क्षेत्र उसी दौर की देन हैं। रायगढ़ ज़िला भी उन दिनों मध्यप्रदेश का हिस्सा था। कलकत्ता से रात भर की दूरी पर स्थित इस स्थान पर कोयला के साथ अन्य खनिजों की प्रचुरता इस स्थान को कोयला आधारित उद्योगों के लिए एक आदर्श स्थान बनाता थी। किन्तु रायगढ़ में राज्य या केंद्र की सरकार की ओर से इस दिशा में किसी भी पहल की सुगबुगाहट नहीं थी। तत्कालीन जनप्रतिनिधियों के सारे प्रयास असफल रहे थे। सरकार की ओर से बताया गया था कि रायगढ़ का नाम चूँकि “ज़ीरो-इंडस्ट्री” ज़िलों की सूची में नहीं है इसलिए इसे किसी प्रोत्साहन का लाभ नहीं मिल सकता। सन् 1985 में रायगढ़ से संसद सदस्य रहीं पुष्पा देवी सिंह ने लोकसभा में आपत्ति दर्ज करायी। केंद्र सरकार के उद्योग मंत्री नारायण दत्त तिवारी ने जवाब दिया कि रायगढ़ में चूँकि एक जूटमिल पहले से स्थापित है इसलिए इस ज़िले को “ज़ीरो-इंडस्ट्री” ज़िले के तमग़े के लिए अयोग्य पाया गया था। पुष्पा देवी सिंह को अच्छी खासी मशक़्क़त करना पड़ी केंद्र को यह समझाने में कि जूटमिल बेशक बंद नहीं है किन्तु चल भी नहीं रही है। केंद्र सरकार ने तर्क स्वीकार किये और रायगढ़ ज़िले का समावेश उद्योग-रहित ज़िलों की सूची में हो पाया। अस्सी का दशक समाप्त होते तक हरियाणा से निकले एक और मारवाड़ी ओम प्रकाश जिंदल रायगढ़ पहुंचे। इस बार पटसन का स्थान कोयले और लौह अयस्क ने लिया। 1989 में जिंदल स्ट्रिप्स नाम से औद्योगिक इकाई स्थापित की गयी। इसके साथ ही रायगढ़ में औद्योगिक विकास के दूसरे अध्याय की शुरुआत भी हुई जो अब तक अनवरत जारी है।